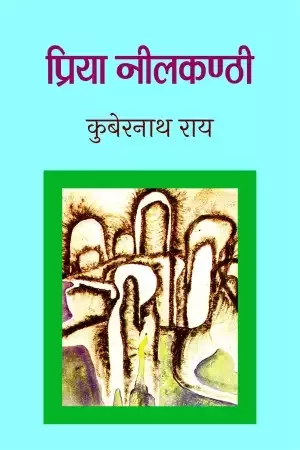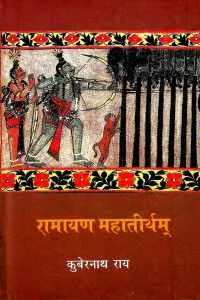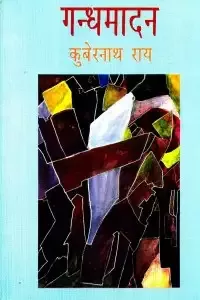|
लेख-निबंध >> प्रिया नीलकण्ठी प्रिया नीलकण्ठीकुबेरनाथ राय
|
23 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है ललित निबन्ध...
Priya Neelkanthi
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय जन-जीवन के परम्परागत पैटर्न में दो रूपान्तरण आज हो रहा है उसकी समग्र अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा ही प्रिया नीलकण्ठी के निबन्धों की सृजन-प्रेरणा है। इस रूपान्तरण में ग्राम-संस्कृति के सूखते रस-बोध का स्थान यन्त्र-युग की बौद्धिकता लेती जा रही है,जिसने आज के व्यक्ति को अभिशप्त और निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश किया है। यह सत्य है कि औद्योगिक संस्कृति के विकास के साथ साथ बौद्धिकता का दायरा बढता जायगा, किन्तु ग्रामीण जीवन की उल्लास साधना इतनी हेय और उपेक्षणीय नहीं कि इसे सूखने दिया जाय।
गूलर के फूल
(एक अरण्य-कथा)
‘‘गूलर का फूल होता है क्या ?’’ बक ने अपने मित्रों की ओर चोंच करके प्रश्न किया।
आज फिर काक, बक और उलूक तीनों मित्र काम्यक वन की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित गूलर के वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए। बगल में ही निर्मल जलवाली पुष्करिणी है जिसमें महाभाग युधिष्ठर स्नान किया करते थे। स्नानोपरान्त कभी-कभी वे इसी गूलर के नीचे बैठकर सहस्रशीर्षा पुरूष विष्णु का ध्यान किया करते थे। और जब कभी-कभी यह ध्यान अति दीर्घकालीन हो जाता और धर्मराज की ललाट पर अरूण तिलक करनेवाली किरणें उनकी पीठ पर पड़ने लगतीं तो भीमसेन भूख से झटपटाकर बेमतलब द्रोपदी से लड़ बैठते थे और नकुल-सहदेव बार-बार देखकर लौट जाते कि भैया की पूजा समाप्त हुई या नहीं। यह गूलर का वृक्ष अति पुरातन था। द्वापर से पूर्व, त्रेता से भी पहले, जब नारायण ने जगत् के उद्धार के लिए नृसिंह वपु धारण किया था तब यह वृक्ष अपनी कुमारावस्था में था। पास ही पार्श्व में एक कटहल का एक नवीन वृक्ष महाबाहु भीमसेन से आरोपित कर दिया था। महापराक्रमी वायुपुत्र लघु आकार वाले फलों को अवेलना की दृष्टि से देखते थे।
यह सत-युगी वृक्ष पुरूष युगों के ज्वार भाटे के बीच मौन साक्षी-सा खड़ा रहा। श्रृंगार, वीर, करूणा आदि नवरसों से परे इसका संन्यासी मन भी कभी-कभी अतीत-माधुरी की स्मृति में विगलित हो उठता था। विशेषतः रात्रि की नीरवता में द्रौपदी की करूणा का उसे ध्यान हो जाता, तो इस युगों में वृद्ध सहचर के हृदय की चीरती हुई एक लम्बी साँस निकल जाती।
इस ‘श्वेत वाराह-कल्पे, कलियुगे’ प्रथम चरण के मध्य में सहस्रानीक अर्जुन के वशंज उदयन का कौशाम्बी में, प्रसेनजित् का अवध में एवं अजातशत्रु का मगध में राज्य चल रहा था, एवं विष्णु के बौद्धावतार का पदार्पण हो चुका था, काम्यक वन की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित इसी गूलर के पेड़ के नीचे बक ने काक और उलूक से पूछा-‘‘गूलर में फूल लगता है क्या ?’’
‘‘हमने तो कभी नहीं देखा भाई! उड्डीन-पड्डीन आदि सताधिक गतियों से ससागरा धरा को कई बार माप डाला पर गूलर का फूल कहीं नहीं मिला। परन्तु मैं दिन की बात कह रहा हूँ। रात की बातों का विशेषज्ञ तो मित्र उलूक है। पूछ कर देखो।’’
‘‘क्यों बन्धु, कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हो ? तुम्हें तो अन्धकार की मायाविनी गतियों का भी परिचय है ।’’
उलूक ने शान्त भाव से उत्तर दिया, ‘‘देखा तो मैंने कभी भी नहीं और न कभी अनुसन्धान करने की चेष्टा ही की। पर बड़ी अचरज की बात है ! भला बिना फूल के फल कैसा होगा ?’’
‘‘काकभुशुण्डि के कुलपत्तिव में मैं गरूड़-जैसे बलवान् और उजड्ड छात्र का सहपाठी था। परन्तु इस विषय पर कोई विशिष्ट सुनने में नहीं आयी। हाँ, मनुष्यों में प्रचलित है कि गूलर का फूल होता है एवं यह आधी रात को खिलता है, अल्प काल के लिए। फिर अन्तर्धान। उस समय यक्षों का इस पर अदृश्य पहरा बैठता है। सुनता हूँ एक बार एक पंखड़ी टूटकर एक दहीवाली हाँड़ी में गिरी, सो दिन-भर वह दही समाप्त नहीं हुआ।’’
‘‘ऐसा ?’’-काक की बुद्धिमत्ता और विचित्र बात सुनकर उन दोनों ने चकित स्वर में कहा।
‘‘तब तो आज रात, भूत हो या प्रेत, यहीं इस बात की जाँच हो जाए।’’ बक ने, जो निरिक्षण का स्वभावतः प्रेमी था, सुझाव दिया।
तीनों साहसी वीरों ने यही निश्चय किया। भगवान सूर्यनारायण अपनी पीत-अरूण आभा से इस धरती को राग-मय कर रहे थे। धीरे-धीरे दबे पाँव श्यामली उतरने लगी। पक्षियों ने थोड़ी देर दुखःसुख की कथा एक दूसरे से कहकर रैन-बसेरा लिया। तारे उगे। रात्रि का कालरथ क्षण-प्रतिक्षण बढ़ता गया। हवा धीमी हो चली। वातावरण से भय और वैराग्य के अनुभवों का संवेदन मिलने लगा। इस भयानक चुप्पी से गूलर की सर्वोच्च शाखा पर ये तीनों मित्र भय और उत्साह की मिश्रित भावदशा में आधी रात के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
ठीक आधी रात को गूलर के तने को चीरती हुई दीर्घ निःश्वास निकली। बक और अन्य दो मित्र सावधान हो गये। इसी समय जम्हाई लेते हुए कटहल ने पूछा, ‘‘दादा, आज क्यों दुःखी ज्ञात होते हो ?’’
‘‘क्या कहूँ ?’’ गूलर ने उत्तर दिया। ‘‘मेरी शाखा पर आज तीन अतिथि आये हैं। विश्राम के लिए नहीं। मेरे मस्तक की शोभा-मेरा पुष्पदल देखने की अभिलाषा से। मैं इन्हें कैसे समझाऊँ ? मेरे पास फूल कहाँ है ? इन्हें निराश लौटना होगा। ऐसा फूल तो कभी नहीं, कहीं नहीं खिला जैसा लोग कहा करते हैं। यह तो मनुष्य लोक के मोह का प्रतिरूप है। मेरा शरीर तो फोड़े की तरह स्वादहीन फलों से लदा है जिन्हें कोई भी जीव नहीं पूछता है क्या कहूँ ? किसी के काम नहीं आया।’’ गूलर ने फिर लम्बी साँस ली।
‘‘दादा, ऐसा क्यों हुआ ? तुम तो बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारी छाया में महाभाग पाण्डवों ने विश्राम किया है। फिर विधाता की ओर से तुम्हें पुण्य का वरदान क्यों नहीं मिला ?’’
‘‘मेरी इस अवस्था का कारण ही कुछ और है। एक समय धरती पर हिरण्यकशिपु का अत्याचार दुःसह हो गया। वेद लुप्त हो गये। ब्राह्मणों की जीभ काट ली गयी, कुछ की शस्त्र से और कुछ की स्वर्ण से। उस समय भक्तवत्सलय विष्णु ने असुर के विनाश के लिए नृसिंह रूप धारण किया। आज भी उस अपूर्व तेजोमय सिंहपुरूष का स्मरण करके रोमांच हो जाता है।’’ गूलर क्षण-भर उस रूप की स्मृति में मौन रहा। फिर आगे बोला, ‘‘असुर का वद करने के पश्चात उनके नखों में भयंकर जलन होने लगी। यह जलन जब किसी उपाय से शान्त न हो पायी तो नारायण पीड़ित होकर हमारे पास आये। तीनों लोकों के त्राता जनार्दन को अपने दरिद्र द्वार पर खड़ा याचना की मुद्रा में देखकर मैं धन्य-धन्य हो गया और उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दिया। उनकी नखज्वाला तो मेरे शरीर में नखों के धँसाने से शान्त हो गयी। परन्तु उस दाह को खींचकर मेरा शरीर विषाक्त हो गया। तभी से फोड़े की तरह फल-व्रण ही मुझमें लगते हैं-पुष्प मुझमें नहीं लगता। फल भी रस हीन और कीटपूर्ण होते हैं !’’
‘‘दादा, तुमने उसके विष को आत्मसात् किया जिसके चरणों से पतितपावनी गंगा निकली है।–तुम्हारे पुष्प, तुम्हारी मस्तक-मणियाँ तुम्हारे अन्तर में हैं। तुमको ही देखकर मुझे भी फूलों का शौक न रहा। मेरे फूल भी नाम मात्र के होते हैं। मैं भी पुष्प माला धारण कर के प्रेमियों का हृदय विगलित करने और जगत् को रिझाने की अपेक्षा परिपुष्टि और दीर्घाकार फल देने की चेष्टा करता हूँ।’’ कटहल ने कहा।
‘‘चरचार को रिझाने से क्या लाभ ? जिन्हें वास्तव में रिझाना है वे तो अन्तर्मन के सौन्दर्य को देखते हैं। औरों से क्या लाभ ?’’ कहकर गूलर मौन हो गया।
बक, काक और उलूक तीनों अलभ्य कुसुम की आशा में आये थे। उससे भी बढ़कर अलभ्य और मनोरमा कुसुम उन्हें मिल गया। तीनों ने मन-ही-मन गुरू और शिष्य दोनों को प्रमाण किया।
आज फिर काक, बक और उलूक तीनों मित्र काम्यक वन की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित गूलर के वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए। बगल में ही निर्मल जलवाली पुष्करिणी है जिसमें महाभाग युधिष्ठर स्नान किया करते थे। स्नानोपरान्त कभी-कभी वे इसी गूलर के नीचे बैठकर सहस्रशीर्षा पुरूष विष्णु का ध्यान किया करते थे। और जब कभी-कभी यह ध्यान अति दीर्घकालीन हो जाता और धर्मराज की ललाट पर अरूण तिलक करनेवाली किरणें उनकी पीठ पर पड़ने लगतीं तो भीमसेन भूख से झटपटाकर बेमतलब द्रोपदी से लड़ बैठते थे और नकुल-सहदेव बार-बार देखकर लौट जाते कि भैया की पूजा समाप्त हुई या नहीं। यह गूलर का वृक्ष अति पुरातन था। द्वापर से पूर्व, त्रेता से भी पहले, जब नारायण ने जगत् के उद्धार के लिए नृसिंह वपु धारण किया था तब यह वृक्ष अपनी कुमारावस्था में था। पास ही पार्श्व में एक कटहल का एक नवीन वृक्ष महाबाहु भीमसेन से आरोपित कर दिया था। महापराक्रमी वायुपुत्र लघु आकार वाले फलों को अवेलना की दृष्टि से देखते थे।
यह सत-युगी वृक्ष पुरूष युगों के ज्वार भाटे के बीच मौन साक्षी-सा खड़ा रहा। श्रृंगार, वीर, करूणा आदि नवरसों से परे इसका संन्यासी मन भी कभी-कभी अतीत-माधुरी की स्मृति में विगलित हो उठता था। विशेषतः रात्रि की नीरवता में द्रौपदी की करूणा का उसे ध्यान हो जाता, तो इस युगों में वृद्ध सहचर के हृदय की चीरती हुई एक लम्बी साँस निकल जाती।
इस ‘श्वेत वाराह-कल्पे, कलियुगे’ प्रथम चरण के मध्य में सहस्रानीक अर्जुन के वशंज उदयन का कौशाम्बी में, प्रसेनजित् का अवध में एवं अजातशत्रु का मगध में राज्य चल रहा था, एवं विष्णु के बौद्धावतार का पदार्पण हो चुका था, काम्यक वन की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर स्थित इसी गूलर के पेड़ के नीचे बक ने काक और उलूक से पूछा-‘‘गूलर में फूल लगता है क्या ?’’
‘‘हमने तो कभी नहीं देखा भाई! उड्डीन-पड्डीन आदि सताधिक गतियों से ससागरा धरा को कई बार माप डाला पर गूलर का फूल कहीं नहीं मिला। परन्तु मैं दिन की बात कह रहा हूँ। रात की बातों का विशेषज्ञ तो मित्र उलूक है। पूछ कर देखो।’’
‘‘क्यों बन्धु, कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हो ? तुम्हें तो अन्धकार की मायाविनी गतियों का भी परिचय है ।’’
उलूक ने शान्त भाव से उत्तर दिया, ‘‘देखा तो मैंने कभी भी नहीं और न कभी अनुसन्धान करने की चेष्टा ही की। पर बड़ी अचरज की बात है ! भला बिना फूल के फल कैसा होगा ?’’
‘‘काकभुशुण्डि के कुलपत्तिव में मैं गरूड़-जैसे बलवान् और उजड्ड छात्र का सहपाठी था। परन्तु इस विषय पर कोई विशिष्ट सुनने में नहीं आयी। हाँ, मनुष्यों में प्रचलित है कि गूलर का फूल होता है एवं यह आधी रात को खिलता है, अल्प काल के लिए। फिर अन्तर्धान। उस समय यक्षों का इस पर अदृश्य पहरा बैठता है। सुनता हूँ एक बार एक पंखड़ी टूटकर एक दहीवाली हाँड़ी में गिरी, सो दिन-भर वह दही समाप्त नहीं हुआ।’’
‘‘ऐसा ?’’-काक की बुद्धिमत्ता और विचित्र बात सुनकर उन दोनों ने चकित स्वर में कहा।
‘‘तब तो आज रात, भूत हो या प्रेत, यहीं इस बात की जाँच हो जाए।’’ बक ने, जो निरिक्षण का स्वभावतः प्रेमी था, सुझाव दिया।
तीनों साहसी वीरों ने यही निश्चय किया। भगवान सूर्यनारायण अपनी पीत-अरूण आभा से इस धरती को राग-मय कर रहे थे। धीरे-धीरे दबे पाँव श्यामली उतरने लगी। पक्षियों ने थोड़ी देर दुखःसुख की कथा एक दूसरे से कहकर रैन-बसेरा लिया। तारे उगे। रात्रि का कालरथ क्षण-प्रतिक्षण बढ़ता गया। हवा धीमी हो चली। वातावरण से भय और वैराग्य के अनुभवों का संवेदन मिलने लगा। इस भयानक चुप्पी से गूलर की सर्वोच्च शाखा पर ये तीनों मित्र भय और उत्साह की मिश्रित भावदशा में आधी रात के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
ठीक आधी रात को गूलर के तने को चीरती हुई दीर्घ निःश्वास निकली। बक और अन्य दो मित्र सावधान हो गये। इसी समय जम्हाई लेते हुए कटहल ने पूछा, ‘‘दादा, आज क्यों दुःखी ज्ञात होते हो ?’’
‘‘क्या कहूँ ?’’ गूलर ने उत्तर दिया। ‘‘मेरी शाखा पर आज तीन अतिथि आये हैं। विश्राम के लिए नहीं। मेरे मस्तक की शोभा-मेरा पुष्पदल देखने की अभिलाषा से। मैं इन्हें कैसे समझाऊँ ? मेरे पास फूल कहाँ है ? इन्हें निराश लौटना होगा। ऐसा फूल तो कभी नहीं, कहीं नहीं खिला जैसा लोग कहा करते हैं। यह तो मनुष्य लोक के मोह का प्रतिरूप है। मेरा शरीर तो फोड़े की तरह स्वादहीन फलों से लदा है जिन्हें कोई भी जीव नहीं पूछता है क्या कहूँ ? किसी के काम नहीं आया।’’ गूलर ने फिर लम्बी साँस ली।
‘‘दादा, ऐसा क्यों हुआ ? तुम तो बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारी छाया में महाभाग पाण्डवों ने विश्राम किया है। फिर विधाता की ओर से तुम्हें पुण्य का वरदान क्यों नहीं मिला ?’’
‘‘मेरी इस अवस्था का कारण ही कुछ और है। एक समय धरती पर हिरण्यकशिपु का अत्याचार दुःसह हो गया। वेद लुप्त हो गये। ब्राह्मणों की जीभ काट ली गयी, कुछ की शस्त्र से और कुछ की स्वर्ण से। उस समय भक्तवत्सलय विष्णु ने असुर के विनाश के लिए नृसिंह रूप धारण किया। आज भी उस अपूर्व तेजोमय सिंहपुरूष का स्मरण करके रोमांच हो जाता है।’’ गूलर क्षण-भर उस रूप की स्मृति में मौन रहा। फिर आगे बोला, ‘‘असुर का वद करने के पश्चात उनके नखों में भयंकर जलन होने लगी। यह जलन जब किसी उपाय से शान्त न हो पायी तो नारायण पीड़ित होकर हमारे पास आये। तीनों लोकों के त्राता जनार्दन को अपने दरिद्र द्वार पर खड़ा याचना की मुद्रा में देखकर मैं धन्य-धन्य हो गया और उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दिया। उनकी नखज्वाला तो मेरे शरीर में नखों के धँसाने से शान्त हो गयी। परन्तु उस दाह को खींचकर मेरा शरीर विषाक्त हो गया। तभी से फोड़े की तरह फल-व्रण ही मुझमें लगते हैं-पुष्प मुझमें नहीं लगता। फल भी रस हीन और कीटपूर्ण होते हैं !’’
‘‘दादा, तुमने उसके विष को आत्मसात् किया जिसके चरणों से पतितपावनी गंगा निकली है।–तुम्हारे पुष्प, तुम्हारी मस्तक-मणियाँ तुम्हारे अन्तर में हैं। तुमको ही देखकर मुझे भी फूलों का शौक न रहा। मेरे फूल भी नाम मात्र के होते हैं। मैं भी पुष्प माला धारण कर के प्रेमियों का हृदय विगलित करने और जगत् को रिझाने की अपेक्षा परिपुष्टि और दीर्घाकार फल देने की चेष्टा करता हूँ।’’ कटहल ने कहा।
‘‘चरचार को रिझाने से क्या लाभ ? जिन्हें वास्तव में रिझाना है वे तो अन्तर्मन के सौन्दर्य को देखते हैं। औरों से क्या लाभ ?’’ कहकर गूलर मौन हो गया।
बक, काक और उलूक तीनों अलभ्य कुसुम की आशा में आये थे। उससे भी बढ़कर अलभ्य और मनोरमा कुसुम उन्हें मिल गया। तीनों ने मन-ही-मन गुरू और शिष्य दोनों को प्रमाण किया।
हेमन्त की सन्ध्या
हेमन्त का सबसे बड़ा आकर्षण है पत्तियों का पीला पड़ जाना और जरा-सी हवा डोलने पर भू-पतित हो जाना। पत्तियों का झरना धरती के सौन्दर्य की करुणतम अवस्था है। करुणा में एक उदास सौन्दर्य की उपलब्धि एक सर्वसाधारण अनुभव है। करुणा विषाद की रोमाण्टिक अवस्था है। वही अनुभूति जब क्रूर रूप में घटित होकर कठोर सत्य बन जाती है तो हम उसे विषाद कहते हैं। मृत्यु का बोध विषाद है, करुणा नहीं। करुणा किसी-न-किसी रूप में जीवन से संलग्न रहती है। इसमें आस्था का एक क्षीण धागा बँधा रहता है।
विषाद में सारे मूल्य अर्थहीन हो जाते हैं। आधुनिक युग को हम विषाद का युग कह सकते हैं। आज जो घटित हो रहा है वह ट्रेजेडी नहीं। ट्रेजेडी से तो मनुष्य का धरातल सदैव ऊंचा उठता है। हमारा युग स्नेह और प्रीति में तो रिक्त है ही, करुणा में भी यह अति दरिद्र है। यह इतना दीन हो चुका है कि इसकी अन्तिम पूँजी-विषाद-भी धीरे-धीरे चुक रही है और इसके शेष हो जाने पर यह आत्मघात से भी बुरी अवस्था होगी।
बात हेमन्त को लेकर चली थी। पीली पत्तियों के उदास सौन्दर्य के बाद उसका दूसरा रूप-विन्यास है धीरे-धीरे उतरती हुई ठण्डी साँस। कमरे में अकेले बैठकर ‘शामेग़म’ का मजा, उदासीनता का रसबोध, निर्मम होते हुए भी नशीला है। रिक्तता में एक स्वाद है। यह सिर्फ लत लग जाने की बात है। बन्द वातायन के बाहर अरुणिमा धीरे-धीरे गलकर घुल चुकी है। पेड़ों के सिर पर ओस की मोटी तह बादलों की-सी जम गयी है, जो क्षण-प्रतिक्षण अंगुल-अंगुल करके नीचे खिसक रही है। परन्तु आँखों से इस क्रमिक आरोहण को हम पकड़ नहीं पाते हैं। धीरे-धीरे कुहासे की प्लावन-धारा पवन की तरंगों पर बहने लगती है। पर धरती का राजमुकुट महान् मनुष्य और सृष्टि के अन्य क्षुद्र जीव वातायन-बद्ध होकर या नीड़-बद्ध होकर अपनी क्षुद्र सीमा में ही अपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन-भर हाट-बाट गली-कूचों की खाक छानने पर भी हम जब अपने को न पा सके-मनचाही उपलब्धि न हो सकी तो जीवन का सारा दैन्य क्षुद्र सीमा में केन्द्रित करके इस बँधी, अर्गला-बद्ध कमरे की दुनिया से आत्म-त्राण की भीख माँग रहे हैं। पर यह अर्गला उन गली-कूचों, पार्कों-मैदानों, सिनेमागृहों और खुले अनन्त विस्तृत नील विमान के तले भी, जो दया करके अपना द्वार सबसे लिए मुक्त खोलकर काल के प्रारम्भ से ही खड़ा है, हमारा पिण्ड छोड़ती है ? हम जहाँ जाते हैं वहीं यह भी है। यह कर्ण के कवच की तरह जन्मजात है। यही हमारी ट्रेजेडी है कि जो हमारे भीतर शिरा-शिरा, धमनी-धमनी बह रही है और बाहर-भीतर भी सब-कुछ को व्याप्त किये है, उस विशाल अन्तर्वाहिनी विभुप्लाविनी को इस लौह-कवच के कारण अस्वीकृत करते चलते हैं। यह बूँद का क्षुद्र अहम् है जो यह अपने को ही धारा मान बैठी और छिटककर दूर जा पड़ी। यह दर्प विषाद की स्थिति है ! आत्मघात है !
अन्धकार भीग गया है। पर गुंजलकबद्ध मैं फन काढ़े बैठा हूँ। स्वयं केन्द्रित। नया मसीहा बोलता है- इस अकेलपन पर, इस अजनबीपन पर। ‘हम अपने ही अजनबी हैं’। मनुष्य को अकेली सत्ता का अभिशाप मिला है। बिना किसी आधार के उसे प्रत्येक पग पर अपने को ढूँढ़कर आविष्कृत करना है। वर्तमान में यह निराधार त्रिशंकु-स्थिति में त्यक्त रूप में है’ (एक्ज़िस्टेन्सियलिज़्म ऐण्ड ह्यूमनिज़्म’-सार्त्र, पृ.34-35)। पर इतना भार बिना किसी का स्नेह-स्पर्श पाये वह कैसे वहन करेगा ? अतीत की भूमि उस के पैरों के नीचे से खिसक गयी-उसका स्वयं भी उससे अजनबी हो गया, तो फिर वह किसका स्नेह-स्पर्श, किसका बल पाकर इतना भार उठाए ? मेरे मित्र, तुम जो नयी ‘फिलॉसफी’ पढ़ते हो, ‘नयी आध्यात्मिकता’ की चर्चा करते हो, नये मूल्यों के सृजन में विश्वकर्मा की तरह लगे हो, मनुष्य के इस संकट को देखकर करुणा क्यों नहीं करते ? पर तुम कहते हो-‘इस विकट स्थिति का निराकण भी है।’
‘क्या ? आत्मघात ?’
‘नहीं,’ तुम्हारा हाथ उसी तरह ऊपर उठ जाता है जैसे बुद्ध ने ‘चरथ भिक्खवे चारिकं..’ कहते समय उठाया था, ‘पूर्ण विप्लव !’ फिर तुम रुक-रुककर आँखें बन्द किये हुए ऐसे बोलते हो गोया कूप गर्त से तुम्हारी आवाज आ रही हो-‘सारे मूल्यों को फिर से गढ़ना होगा। नये सिरे से ! नयी विधा, नयी कवि-प्रसिद्धियाँ और सर्वथा नवीन पद्धति के द्वारा व्यक्ति को ‘पूर्ण व्यक्ति’ करना होगा। सबसे अलग, सबसे मुक्त !’
‘ओह ! समझा ! अरविन्द...’
‘नहीं, नहीं, नहीं !’ तुम चौंककर कहते हो-‘अतिमा में-ट्रान्सेण्डेन्स में, हमारा विश्वास नहीं। अध्यात्म का पुराना हल हमारे काम का नहीं।’
पर ‘फूलहिं फरहिं न बेंत जदपि सुधा बरसहिं जलद।’ विरंचि-जैसा गुरु मिलने पर भी हम-जैसों को चेत कहाँ से आएगा। बात की ग्रन्थि जैसी थी वैसी ही रह गयी।
इतने में कोई लालटेन रख जाता है। प्रकाश मुझे उस गुंजलक से मुक्त कर देता है।
’इस साल भी अरहर गयी। ऐसा पाला तो कभी पड़ा ही नहीं था। रबी की फसल भी आधी चौपट हो गयी।’
इस वैशम्यापन-उवाच के बाद बड़का बाबा चिलम में तम्बाकू भरने लगे। बाहर नीम की छाया में अलाव जला है। किसी ने सूखे घास-फूस की नयी आहुति दी और लपट लप-लप कर के ऊंची चढ़ने लगी। ऊपर की पत्तियाँ थर-थर काँप उठीं और कुछ तो पुण्य-क्षीण आत्माओं की तरह उस अग्निशिखा में टूट-टूटकर गिरने लगीं। आबालवृद्ध सबके मुख पर प्रसन्नता छा गयी। जीवन में प्रसन्नता के क्षण बहुत ही महँगे होते हैं। ऐसे मामूली क्षणों का भी अमित मोल है जो हलकी-सी ऊष्मा के द्वारा देह-मन को स्फूर्त या पुलकित कर देते हैं। बाबा ने चिलम भरकर कहा, ‘इस वर्ष अगहनी भी गायब ही रही। क्या जमाना है ! जिन खेतों में बारह मन बीघे काटा था उनमें दो मन बीघा किसी तरह से गया।’ इसके बाद तो बातों का सिलसिला चला। भाग्य-दैव को कोसने के बाद अगल-बगल की परिषद् ने अनेक प्रश्नों यथा-ग्राम-सेवक, पंचवार्षिक योजना, नगर विभाग की बदमाशी, चीनी आक्रमण, विलायती खाद की व्यर्थता और फिर चीनी का अभाव आदि-आदि पर अस्त-व्यस्त टीका-टिप्पणी की। साथ-साथ गाँव के ‘उत्तम’ चरित्रों की चर्चा और परनिन्दा की चाशनी ने उक्त शुष्क विषयों को मीठा, नमकीन और फिर तिक्त बनाया। पर समस्त प्रक्रिया में बाबा या तो चुप रहे, नहीं तो ‘हाँ, हूँ’ मात्र करते रहे। खेती-बारी से आगे उनके दो ही राजनीतिक विषय हैं। एक तो सन् ‘सत्तावन की गदर में अपने पितामह की करतूतों का विशद वर्णन और दूसरी सन् ‘चौदह की लड़ाई, जिसमें स्वयं सैनिक बनकर भरती हुए थे परन्तु मोरचे का मुँह नहीं देखा और सारी वीरता हवलदारों और सूबेदारों से भिड़न्त तक ही सीमित रही, जो स्वभाववश अकसर हो जाती थी। कांग्रेस की राजनीति में उन्हें अरुचि है। इसका एक व्यक्तिगत कारण है। अपने लघुभ्राता को महाकष्ट उठाकर बारह वर्ष तक पढ़ने का खर्च कलकत्ते भेजते रहे और वे सज्जन इन की आँखों पर पट्टी बाँधकर पढ़ाई-लिखाई के नाम पर देश-भक्ति (बाबा के शब्दों में ‘आवारागरदी’) करते रहे। स्वामी सत्यदेव का नाम किसी तरह से जान गये हैं और कहा करते हैं, ‘सतदेउआ’ ने हमारा घर बिगाड़ दिया। गाँधीजी पर उनके मरने के बाद इनकी श्रद्धा बढ़ी है। पर वह बापू की राजनीतिक क्षमता के कारण नहीं। उन की राम-भक्ति के कारण उनको ये ‘ऋषि’ मानने लगे हैं। प्रमाण में तुलसीदास को उद्धृत किया करते हैं-
विषाद में सारे मूल्य अर्थहीन हो जाते हैं। आधुनिक युग को हम विषाद का युग कह सकते हैं। आज जो घटित हो रहा है वह ट्रेजेडी नहीं। ट्रेजेडी से तो मनुष्य का धरातल सदैव ऊंचा उठता है। हमारा युग स्नेह और प्रीति में तो रिक्त है ही, करुणा में भी यह अति दरिद्र है। यह इतना दीन हो चुका है कि इसकी अन्तिम पूँजी-विषाद-भी धीरे-धीरे चुक रही है और इसके शेष हो जाने पर यह आत्मघात से भी बुरी अवस्था होगी।
बात हेमन्त को लेकर चली थी। पीली पत्तियों के उदास सौन्दर्य के बाद उसका दूसरा रूप-विन्यास है धीरे-धीरे उतरती हुई ठण्डी साँस। कमरे में अकेले बैठकर ‘शामेग़म’ का मजा, उदासीनता का रसबोध, निर्मम होते हुए भी नशीला है। रिक्तता में एक स्वाद है। यह सिर्फ लत लग जाने की बात है। बन्द वातायन के बाहर अरुणिमा धीरे-धीरे गलकर घुल चुकी है। पेड़ों के सिर पर ओस की मोटी तह बादलों की-सी जम गयी है, जो क्षण-प्रतिक्षण अंगुल-अंगुल करके नीचे खिसक रही है। परन्तु आँखों से इस क्रमिक आरोहण को हम पकड़ नहीं पाते हैं। धीरे-धीरे कुहासे की प्लावन-धारा पवन की तरंगों पर बहने लगती है। पर धरती का राजमुकुट महान् मनुष्य और सृष्टि के अन्य क्षुद्र जीव वातायन-बद्ध होकर या नीड़-बद्ध होकर अपनी क्षुद्र सीमा में ही अपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन-भर हाट-बाट गली-कूचों की खाक छानने पर भी हम जब अपने को न पा सके-मनचाही उपलब्धि न हो सकी तो जीवन का सारा दैन्य क्षुद्र सीमा में केन्द्रित करके इस बँधी, अर्गला-बद्ध कमरे की दुनिया से आत्म-त्राण की भीख माँग रहे हैं। पर यह अर्गला उन गली-कूचों, पार्कों-मैदानों, सिनेमागृहों और खुले अनन्त विस्तृत नील विमान के तले भी, जो दया करके अपना द्वार सबसे लिए मुक्त खोलकर काल के प्रारम्भ से ही खड़ा है, हमारा पिण्ड छोड़ती है ? हम जहाँ जाते हैं वहीं यह भी है। यह कर्ण के कवच की तरह जन्मजात है। यही हमारी ट्रेजेडी है कि जो हमारे भीतर शिरा-शिरा, धमनी-धमनी बह रही है और बाहर-भीतर भी सब-कुछ को व्याप्त किये है, उस विशाल अन्तर्वाहिनी विभुप्लाविनी को इस लौह-कवच के कारण अस्वीकृत करते चलते हैं। यह बूँद का क्षुद्र अहम् है जो यह अपने को ही धारा मान बैठी और छिटककर दूर जा पड़ी। यह दर्प विषाद की स्थिति है ! आत्मघात है !
अन्धकार भीग गया है। पर गुंजलकबद्ध मैं फन काढ़े बैठा हूँ। स्वयं केन्द्रित। नया मसीहा बोलता है- इस अकेलपन पर, इस अजनबीपन पर। ‘हम अपने ही अजनबी हैं’। मनुष्य को अकेली सत्ता का अभिशाप मिला है। बिना किसी आधार के उसे प्रत्येक पग पर अपने को ढूँढ़कर आविष्कृत करना है। वर्तमान में यह निराधार त्रिशंकु-स्थिति में त्यक्त रूप में है’ (एक्ज़िस्टेन्सियलिज़्म ऐण्ड ह्यूमनिज़्म’-सार्त्र, पृ.34-35)। पर इतना भार बिना किसी का स्नेह-स्पर्श पाये वह कैसे वहन करेगा ? अतीत की भूमि उस के पैरों के नीचे से खिसक गयी-उसका स्वयं भी उससे अजनबी हो गया, तो फिर वह किसका स्नेह-स्पर्श, किसका बल पाकर इतना भार उठाए ? मेरे मित्र, तुम जो नयी ‘फिलॉसफी’ पढ़ते हो, ‘नयी आध्यात्मिकता’ की चर्चा करते हो, नये मूल्यों के सृजन में विश्वकर्मा की तरह लगे हो, मनुष्य के इस संकट को देखकर करुणा क्यों नहीं करते ? पर तुम कहते हो-‘इस विकट स्थिति का निराकण भी है।’
‘क्या ? आत्मघात ?’
‘नहीं,’ तुम्हारा हाथ उसी तरह ऊपर उठ जाता है जैसे बुद्ध ने ‘चरथ भिक्खवे चारिकं..’ कहते समय उठाया था, ‘पूर्ण विप्लव !’ फिर तुम रुक-रुककर आँखें बन्द किये हुए ऐसे बोलते हो गोया कूप गर्त से तुम्हारी आवाज आ रही हो-‘सारे मूल्यों को फिर से गढ़ना होगा। नये सिरे से ! नयी विधा, नयी कवि-प्रसिद्धियाँ और सर्वथा नवीन पद्धति के द्वारा व्यक्ति को ‘पूर्ण व्यक्ति’ करना होगा। सबसे अलग, सबसे मुक्त !’
‘ओह ! समझा ! अरविन्द...’
‘नहीं, नहीं, नहीं !’ तुम चौंककर कहते हो-‘अतिमा में-ट्रान्सेण्डेन्स में, हमारा विश्वास नहीं। अध्यात्म का पुराना हल हमारे काम का नहीं।’
पर ‘फूलहिं फरहिं न बेंत जदपि सुधा बरसहिं जलद।’ विरंचि-जैसा गुरु मिलने पर भी हम-जैसों को चेत कहाँ से आएगा। बात की ग्रन्थि जैसी थी वैसी ही रह गयी।
इतने में कोई लालटेन रख जाता है। प्रकाश मुझे उस गुंजलक से मुक्त कर देता है।
’इस साल भी अरहर गयी। ऐसा पाला तो कभी पड़ा ही नहीं था। रबी की फसल भी आधी चौपट हो गयी।’
इस वैशम्यापन-उवाच के बाद बड़का बाबा चिलम में तम्बाकू भरने लगे। बाहर नीम की छाया में अलाव जला है। किसी ने सूखे घास-फूस की नयी आहुति दी और लपट लप-लप कर के ऊंची चढ़ने लगी। ऊपर की पत्तियाँ थर-थर काँप उठीं और कुछ तो पुण्य-क्षीण आत्माओं की तरह उस अग्निशिखा में टूट-टूटकर गिरने लगीं। आबालवृद्ध सबके मुख पर प्रसन्नता छा गयी। जीवन में प्रसन्नता के क्षण बहुत ही महँगे होते हैं। ऐसे मामूली क्षणों का भी अमित मोल है जो हलकी-सी ऊष्मा के द्वारा देह-मन को स्फूर्त या पुलकित कर देते हैं। बाबा ने चिलम भरकर कहा, ‘इस वर्ष अगहनी भी गायब ही रही। क्या जमाना है ! जिन खेतों में बारह मन बीघे काटा था उनमें दो मन बीघा किसी तरह से गया।’ इसके बाद तो बातों का सिलसिला चला। भाग्य-दैव को कोसने के बाद अगल-बगल की परिषद् ने अनेक प्रश्नों यथा-ग्राम-सेवक, पंचवार्षिक योजना, नगर विभाग की बदमाशी, चीनी आक्रमण, विलायती खाद की व्यर्थता और फिर चीनी का अभाव आदि-आदि पर अस्त-व्यस्त टीका-टिप्पणी की। साथ-साथ गाँव के ‘उत्तम’ चरित्रों की चर्चा और परनिन्दा की चाशनी ने उक्त शुष्क विषयों को मीठा, नमकीन और फिर तिक्त बनाया। पर समस्त प्रक्रिया में बाबा या तो चुप रहे, नहीं तो ‘हाँ, हूँ’ मात्र करते रहे। खेती-बारी से आगे उनके दो ही राजनीतिक विषय हैं। एक तो सन् ‘सत्तावन की गदर में अपने पितामह की करतूतों का विशद वर्णन और दूसरी सन् ‘चौदह की लड़ाई, जिसमें स्वयं सैनिक बनकर भरती हुए थे परन्तु मोरचे का मुँह नहीं देखा और सारी वीरता हवलदारों और सूबेदारों से भिड़न्त तक ही सीमित रही, जो स्वभाववश अकसर हो जाती थी। कांग्रेस की राजनीति में उन्हें अरुचि है। इसका एक व्यक्तिगत कारण है। अपने लघुभ्राता को महाकष्ट उठाकर बारह वर्ष तक पढ़ने का खर्च कलकत्ते भेजते रहे और वे सज्जन इन की आँखों पर पट्टी बाँधकर पढ़ाई-लिखाई के नाम पर देश-भक्ति (बाबा के शब्दों में ‘आवारागरदी’) करते रहे। स्वामी सत्यदेव का नाम किसी तरह से जान गये हैं और कहा करते हैं, ‘सतदेउआ’ ने हमारा घर बिगाड़ दिया। गाँधीजी पर उनके मरने के बाद इनकी श्रद्धा बढ़ी है। पर वह बापू की राजनीतिक क्षमता के कारण नहीं। उन की राम-भक्ति के कारण उनको ये ‘ऋषि’ मानने लगे हैं। प्रमाण में तुलसीदास को उद्धृत किया करते हैं-
‘‘जनम जनम मुनि जतन कराहीं।
अन्त राम कहि पावत नाहीं।।’’
अन्त राम कहि पावत नाहीं।।’’
वैशम्पायन तो प्रथम सूत्र के उवाच के पश्चात् चुप रहे। प्रधान वार्ता तो अनेक जनमेजयों के द्वारा हुई जो उस परिषद् की शोभा बढ़ा रहे थे। मेरे मन में चिरकाल से जलनेवाले इस अलाव के साक्ष्य में गाथा-गान करनेवाले वैशम्यापनों की मुखाकृतियाँ घूम गयीं। तहसीली के सहदेवराम चपरासी की बड़ी-सी पगड़ी अब भी याद है। वे मेरे बचपन में महाभारत की कथाएँ अपनी पूरी योग्यता का उपयोग करके सुनाते थे। उन दिनों इस बात की पूरी जानकारी रखता था कि किस योद्धा ने किस बाण का प्रहार किस अवस्था में किया। मित्रों में इस जानकारी के बल पर मैं विद्वान भी गिना जाता था। इस जानकारी का प्रारम्भिक श्रेय सहदेवराम को है। दूसरे स्रोत हैं गीता प्रेस के महाभारत का भाषा-संस्करण और सबलसिंह चौहान का ‘महाभारत’। एक समय था कि उत्तर प्रदेश के गाँवों में तुलसीदास के रामायण के बाद सबलसिंह का ही पाठ होता था। हमारे यहाँ सबलसिंह चौहान के सर्वोत्तम वाचक थे पड़ोसी गाँव के ठाकुर घुरहूसिंह। उस वृद्ध का विशाल वपु, रजपूती चाल और वृद्धावस्था में भाला लगाकर चलने का मोह अब भी याद है। बाबा से उनकी खूब पटती थी। देहात में वे ‘आल्हा’ के विद्वान माने जाते थे। उन्हीं की बदौलत मेरे गाँव में और आस-पास के गाँवों में लोगों का विश्वास है कि अब भी विन्ध्याचल की किसी गुफा में दो अमर आत्माएँ एक साथ रह रही हैं-आल्हा और अमरसिंह जो सन् सत्तावनवाले कुँअरसिंह के भाई हैं।
आज वह वीरगाथा युग नहीं रहा। उस परम्परा का ध्वंस बहुत पहले ही हो गया। परन्तु वीरगाथा-युग का अभिमान अभी कल तक नहीं मरा था। पूँजीवादी संस्कृति के संस्कार अब भी ठीक तौर पर जम नहीं पाये हैं। पर इतना तो निश्चय है कि युगधर्म बदल रहा है। आज नहीं तो कल हम अपने को दूसरे रूप में पाएँगे। ग्राम-संस्कृति और वीरगाथा-काल दोनों की सम्पूर्ण मृत्यु-साथ ही साथ होगी। अब अधिक देर नहीं। परन्तु यह भी लगता है कि ग्राम-संस्कृति के महल पर जिन मध्यवर्गीय संस्कारों का महल खड़ा हो रहा है वह अति भयावह वंचना का दुर्ग है। प्रजातान्त्रिक पद्धति के द्वारा ‘नायकों’ की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ‘नायकत्व’ का मापदण्ड वीरगाथाकालीन ‘हीरोइक’ या सामन्तवादी आदर्शों पर आधारित है। पर उसके स्थान पर स्थापित व्यक्ति अपने को भूफोड़ एवं स्वतन्त्र मानकर स्थिति भयावह कर देगा। वीरगाथाकालीन संस्कारों और ग्राम-संस्कारों में व्यक्ति किसी नायक के सम्मुख नल-मस्तक होते हुए भी अपने को पूरे समाज से संयुक्त किये हुए था। वह व्यक्तिवादी नहीं था। लेकिन मध्यवर्गीय संस्कृति का पोषित व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र सत्ता का हुंकार करता है। इसी से आज कोई जनमेजय नहीं, सभी वैशम्पायन-ही-वैशम्पायन हैं। (नायक से मेरा तात्पर्य किसी राजा-जमींदार से नहीं बल्कि अतीत के ‘चरित-नायकों’ या ‘राष्ट्रीय नायकों’ से है। एक समय था कि महात्मा गाँधी ऐसे चरित-नायक की भूमिका निभा रहे थे।)
राष्ट्रीय जीवन की यह ट्रेजेडी दोहरी है। एक ओर ‘व्यक्ति’ है जो बुद्धिवाद का जामा-जोड़ा पहनकर मिथ्या स्वांग का खूब रस ले रहा है और घूम-घूमकर अजनबी बनने का विज्ञापन कर रहा है। ‘मेरी ओर देखो मैं अजनबी हूँ। मेरे पास सिर ही है, धड़ नहीं। मेरी ओर देखो मैं कितना महान् हूँ, क्योंकि मैं अजनबी हूँ। खूबी तो यह है कि इस बुद्धिवाद के जामे में वह डूब सा गया है और अपने को प्रत्येक दशा में प्रेत-सरीखा प्रस्तुत करने में ही अपनी महत्तम पूजा और महत्तम सिद्धि समझ रहा है। दूसरी ओर सामूहिक जीवन का दीन-नग्न कबन्ध है। इस कबन्ध पर ‘स्टेट’ जो उस बुद्धिवादी राहु का रिश्तेदार बन गया है, एक मानवीय-अमानवीय सिर काटकर चस्पाँ करने की सोच रहा है, पर स्वत: इसके साथ संयुक्त होने में इसे अपनी तौहीनी नजर आ रही है। पता नहीं यह नवीन शीश इस दीन-हीन कबन्ध को विनायक बनाएगा अथवा यह दशमुख रावण का मूर्द्धाभिषिक्त ग्यारहवाँ शीश होगा।
हेमन्त की करुणामयी उदास सन्ध्या ने इस प्रश्न को उठाया है। परन्तु उत्तर ?
आज वह वीरगाथा युग नहीं रहा। उस परम्परा का ध्वंस बहुत पहले ही हो गया। परन्तु वीरगाथा-युग का अभिमान अभी कल तक नहीं मरा था। पूँजीवादी संस्कृति के संस्कार अब भी ठीक तौर पर जम नहीं पाये हैं। पर इतना तो निश्चय है कि युगधर्म बदल रहा है। आज नहीं तो कल हम अपने को दूसरे रूप में पाएँगे। ग्राम-संस्कृति और वीरगाथा-काल दोनों की सम्पूर्ण मृत्यु-साथ ही साथ होगी। अब अधिक देर नहीं। परन्तु यह भी लगता है कि ग्राम-संस्कृति के महल पर जिन मध्यवर्गीय संस्कारों का महल खड़ा हो रहा है वह अति भयावह वंचना का दुर्ग है। प्रजातान्त्रिक पद्धति के द्वारा ‘नायकों’ की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ‘नायकत्व’ का मापदण्ड वीरगाथाकालीन ‘हीरोइक’ या सामन्तवादी आदर्शों पर आधारित है। पर उसके स्थान पर स्थापित व्यक्ति अपने को भूफोड़ एवं स्वतन्त्र मानकर स्थिति भयावह कर देगा। वीरगाथाकालीन संस्कारों और ग्राम-संस्कारों में व्यक्ति किसी नायक के सम्मुख नल-मस्तक होते हुए भी अपने को पूरे समाज से संयुक्त किये हुए था। वह व्यक्तिवादी नहीं था। लेकिन मध्यवर्गीय संस्कृति का पोषित व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र सत्ता का हुंकार करता है। इसी से आज कोई जनमेजय नहीं, सभी वैशम्पायन-ही-वैशम्पायन हैं। (नायक से मेरा तात्पर्य किसी राजा-जमींदार से नहीं बल्कि अतीत के ‘चरित-नायकों’ या ‘राष्ट्रीय नायकों’ से है। एक समय था कि महात्मा गाँधी ऐसे चरित-नायक की भूमिका निभा रहे थे।)
राष्ट्रीय जीवन की यह ट्रेजेडी दोहरी है। एक ओर ‘व्यक्ति’ है जो बुद्धिवाद का जामा-जोड़ा पहनकर मिथ्या स्वांग का खूब रस ले रहा है और घूम-घूमकर अजनबी बनने का विज्ञापन कर रहा है। ‘मेरी ओर देखो मैं अजनबी हूँ। मेरे पास सिर ही है, धड़ नहीं। मेरी ओर देखो मैं कितना महान् हूँ, क्योंकि मैं अजनबी हूँ। खूबी तो यह है कि इस बुद्धिवाद के जामे में वह डूब सा गया है और अपने को प्रत्येक दशा में प्रेत-सरीखा प्रस्तुत करने में ही अपनी महत्तम पूजा और महत्तम सिद्धि समझ रहा है। दूसरी ओर सामूहिक जीवन का दीन-नग्न कबन्ध है। इस कबन्ध पर ‘स्टेट’ जो उस बुद्धिवादी राहु का रिश्तेदार बन गया है, एक मानवीय-अमानवीय सिर काटकर चस्पाँ करने की सोच रहा है, पर स्वत: इसके साथ संयुक्त होने में इसे अपनी तौहीनी नजर आ रही है। पता नहीं यह नवीन शीश इस दीन-हीन कबन्ध को विनायक बनाएगा अथवा यह दशमुख रावण का मूर्द्धाभिषिक्त ग्यारहवाँ शीश होगा।
हेमन्त की करुणामयी उदास सन्ध्या ने इस प्रश्न को उठाया है। परन्तु उत्तर ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book